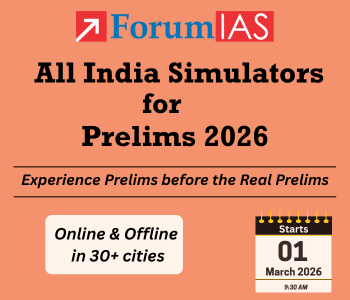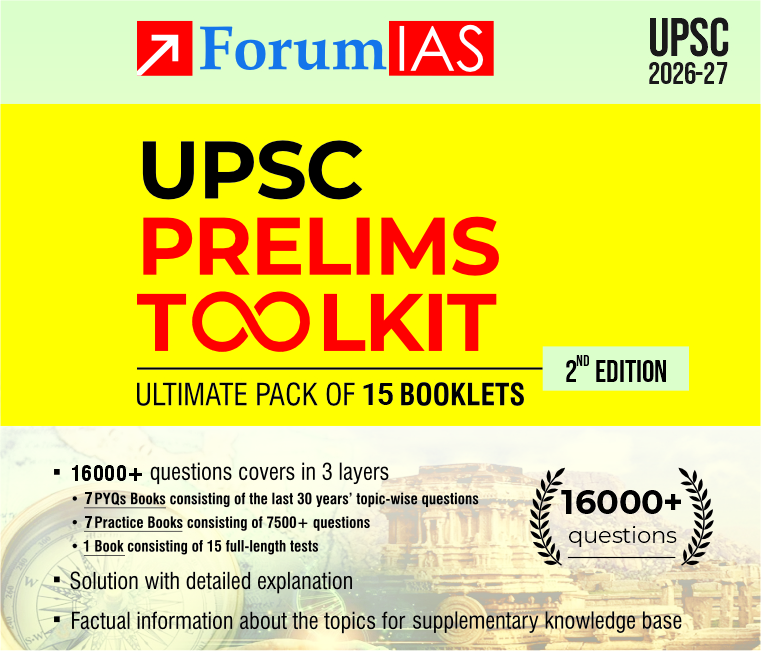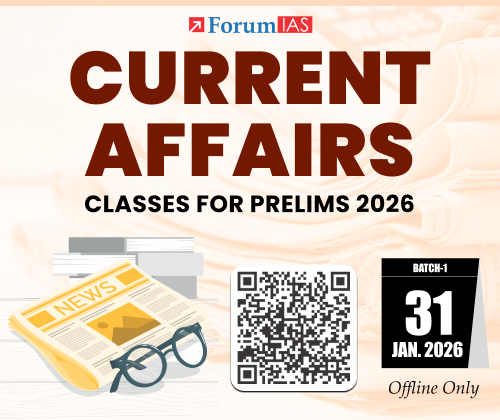भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) डिजिटल परिवर्तन के लिए एक अग्रणी मॉडल के रूप में उभरा है, जिसने वैश्विक ध्यान और प्रशंसा प्राप्त की है, विशेष रूप से भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। देश के DPI की व्यापकता और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता के लिए प्रशंसा की गई है। बिल गेट्स जैसी प्रमुख हस्तियों ने सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत के प्रयासों को मान्यता दी है।

देश का DPI मॉडल, ओपन-सोर्स, इंटरऑपरेबल सिस्टम के इर्द-गिर्द संरचित है, जिसे दुनिया भर के देशों, खासकर ग्लोबल साउथ में तेजी से अपनाया जा रहा है। यह लेख भारत की DPI को वैश्विक बनाने की यात्रा, इसके मुख्य घटकों, लाभों, वैश्विक मान्यता और इसे आगे बढ़ाने में चुनौतियों और अवसरों पर विस्तार से चर्चा करता है।

कंटेंट टेबल
भारत का DPI क्या है?
भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक व्यापक प्रणाली है जिसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से समावेशी और न्यायसंगत विकास को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। “डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर G20 टास्क फोर्स” के अनुसार, DPI को एक अवसंरचना-आधारित दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है जो सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। यह सार्वजनिक हित में निर्मित प्रौद्योगिकी, बाज़ारों और शासन से युक्त एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऐसा करता है, साथ ही नियामक सुरक्षा के भीतर निजी नवाचार की अनुमति भी देता है।
भारत का DPI तीन परस्पर संबद्ध परतों पर बना है, जिन्हें सामूहिक रूप से “इंडिया स्टैक” कहा जाता है:
- पहचान परत: इसमें आधार, भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली, ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) और अन्य प्रणालियाँ शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहचान सत्यापित करती हैं।
- भुगतान परत: इसमें UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफेस), आधार भुगतान ब्रिज और अन्य भुगतान प्रणालियाँ शामिल हैं जो डिजिटल वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं।
- डेटा गवर्नेंस लेयर: इसमें डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं , जो सुरक्षित दस्तावेज़ भंडारण को सक्षम बनाता है, और अकाउंट एग्रीगेटर, जो गोपनीयता के प्रति सजग तरीके से डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
इंडिया स्टैक के मुख्य घटक
भारत के DPI का आधार, इंडिया स्टैक, कई प्रमुख घटकों से मिलकर बना है, जिन्होंने सामूहिक रूप से नागरिकों के सरकारी सेवाओं और निजी क्षेत्र के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है:
- आधार: एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल पहचान अवसंरचना, आधार नागरिकों को उनकी पहचान को एक विशिष्ट संख्या से जोड़कर सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
- UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस): एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली जो मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण को सक्षम बनाती है।
- ई-केवाईसी: कागज रहित पहचान सत्यापन के लिए एक डिजिटल समाधान, जो प्रक्रियाओं को तेज और अधिक कुशल बनाता है।
- डिजिलॉकर : दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहीत और साझा करने के लिए एक सुरक्षित मंच।
- ई-साइन : एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ढांचा जो कागज रहित समझौतों और लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।
- डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण वास्तुकला (DEPA): एक प्रणाली जो व्यक्तियों को अपने डेटा को नियंत्रित करने की अनुमति देती है, सेवा प्रदाताओं के साथ डेटा साझा करते समय गोपनीयता सुनिश्चित करती है।
भारत के डीपीआई का विकास और प्रभाव क्या रहा है?
- उत्पत्ति और विस्तार: भारत की DPI यात्रा 2009 में आधार के लॉन्च के साथ शुरू हुई, जिसने डिजिटल पहचान पहल की शुरुआत की। समय के साथ, इस पहल का विस्तार UPI, JAM (जन धन योजना, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी और Co-WIN जैसे प्लेटफ़ॉर्म को शामिल करने के लिए हुआ, जो भारत के COVID-19 टीकाकरण अभियान के प्रबंधन में महत्वपूर्ण था।
- वित्तीय समावेशन सफलता – भारत के DPI की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में है । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत ने छह वर्षों के भीतर 80% वित्तीय समावेशन हासिल किया – एक उपलब्धि जो, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के एक अध्ययन के अनुसार, अन्यथा 47 साल लग जाते। यह तेज़ वित्तीय समावेशन काफी हद तक सरकारी कल्याण कार्यक्रमों और वित्तीय सेवाओं के साथ आधार के एकीकरण के कारण है।
- क्षेत्रीय प्रभाव – वित्तीय समावेशन से परे, DPI ने स्वास्थ्य सेवा , शिक्षा और स्थिरता जैसे क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है , जिससे बड़े पैमाने पर चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिली है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाओं तक पहुँचने की क्षमता ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।
भारत की डीपीआई की प्रमुख विशेषताएं और लाभ क्या हैं?
भारत के DPI मॉडल की कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अनुकूलनीय, मापनीय और कुशल बनाती हैं:
- ओपन सोर्स और ओपन API: भारत के DPIकी ओपन-सोर्स प्रकृति पारदर्शिता और सहयोग की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार किया जा सकता है और नई चुनौतियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। ओपन एपीआई तीसरे पक्ष के डेवलपर्स को अभिनव समाधान बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
- अंतरसंचालनीयता: अंतरसंचालनीयता पर DPI का फोकस यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म और प्रणालियां आपस में संवाद कर सकें और एक साथ काम कर सकें, जिससे विभिन्न सार्वजनिक और निजी सेवाओं में निर्बाध एकीकरण संभव हो सके।
- डिजाइन द्वारा गोपनीयता: गोपनीयता भारत के DPI का एक मुख्य सिद्धांत है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं कि व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित है। डिजिलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर जैसे प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तियों को अपने डेटा पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देते हैं, जिससे डिजिटल सेवाओं में भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ता है।
- समावेशी डिजाइन और सार्वभौमिक पहुंच: डीपीआई को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए बनाया गया है, जिसमें महिलाओं, ग्रामीण आबादी और विकलांग लोगों जैसे हाशिए के समूह शामिल हैं। इसका डिज़ाइन डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जो असमानताओं को कम करने में सहायक रहा है।
- नवाचार और पारदर्शिता को बढ़ावा देना: विक्रेता लॉक-इन को रोककर और सहयोग को बढ़ावा देकर, DPI नवाचार, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। तीसरे पक्ष की सेवाओं और प्लेटफार्मों को एकीकृत करने की क्षमता ने भारत में एक जीवंत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।
वैश्विक मान्यता क्या है और भारत की डीपीआई से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
- वैश्विक मान्यता: भारत के DPI को G20 के दौरान प्रमुखता मिली, जहाँ फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने UPI जैसे प्लेटफ़ॉर्म की सराहना की। विकासशील देशों, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) ने अपनी डिजिटल यात्रा को गति देने के लिए भारत के DPI को अपनाने में गहरी रुचि व्यक्त की है।
- अंतर्राष्ट्रीय अपनापन: आठ देशों – आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ, बारबाडोस, त्रिनिदाद और टोबैगो, पापुआ न्यू गिनी और मॉरीशस – ने भारत के डीपीआई को बिना किसी लागत और खुले स्रोत तक पहुंच के साथ अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- समर्थन: शुरुआती ठंडी प्रतिक्रियाओं के बावजूद, विकसित देशों ने धीरे-धीरे DPI वैश्वीकरण का समर्थन किया। उदाहरण के लिए क्वाड ने DPI सिद्धांतों का समर्थन किया।
- संयुक्त राष्ट्र की मान्यता: संयुक्त राष्ट्र ने DPI को अपने वैश्विक डिजिटल समझौते में प्राथमिकता के रूप में शामिल किया है, तथा प्रौद्योगिकी के लिए विशेष दूत ने डीपीआई विकास को मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं।
- DPI एज़ अ सर्विस (DaaS): भारत द्वारा एक नया समाधान
a. भारत ने “DaaS” मॉडल पेश किया, जो क्लाउड समाधान के रूप में प्री-पैकेज्ड DPI बिल्डिंग ब्लॉक्स की पेशकश करता है। यह दृष्टिकोण सीमित तकनीकी क्षमता वाले छोटे देशों को किफायती और कुशलतापूर्वक DPI अपनाने में सक्षम बनाता है।
b. 2024 में सहयोगात्मक प्रयासों को हाइपरस्केलर्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स से समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे DaaS मॉडल एक व्यावहारिक विकल्प बन गया।
DPI के वैश्वीकरण में चुनौतियाँ
भारत की DPI को व्यापक रूप से अपनाए जाने के बावजूद, वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव को बढ़ाने में कई चुनौतियाँ हैं:
- तैनाती की जटिलता: DPI सिस्टम को तैनात करने के लिए एक जिम्मेदार सरकारी विभाग की पहचान करना, समाधान डिजाइन करना, उन्हें मौजूदा प्रशासनिक प्रणालियों के साथ एकीकृत करना और उन्हें पूरे देश में लागू करना आवश्यक है। सीमित प्रशासनिक क्षमता वाले देशों को इस संबंध में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
- वैश्विक शासन और गोपनीयता: विभिन्न देशों में निर्बाध DPI अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक शासन संरचना और मानकीकृत विनियमों की अत्यधिक आवश्यकता है। जबकि गोपनीयता DPI का एक मूलभूत सिद्धांत है, डेटा सुरक्षा के बारे में वैश्विक चिंताओं को संबोधित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
आगे का रास्ता: DPI की वैश्विक उन्नति के लिए “ग्लोबल DPI”
G: वैश्विक दक्षिण फोकस: समान चुनौतियों का सामना कर रहे विकासशील देशों के साथ साझेदारी और ज्ञान साझाकरण को प्राथमिकता देना।
L: नेतृत्व और सहयोग: DPI विकास पर वैश्विक नेतृत्व विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
O: खुले मानक और अंतरसंचालनीयता: सीमाओं के पार निर्बाध एकीकरण और मापनीयता सुनिश्चित करने के लिए खुले मानकों और अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना।
B: विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण: पारदर्शी और समावेशी सहभागिता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच विश्वास और भरोसा पैदा करना।
A: अनुकूलन एवं अनुकूलन: विभिन्न देशों और क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और संदर्भों के अनुरूप DPI समाधान तैयार करना।
L: प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: DPI की दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए AI, ब्लॉकचेन और बड़े डेटा जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें।
D: लोकतांत्रिक शासन: सुनिश्चित करें कि DPI का विकास और कार्यान्वयन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो और मानवाधिकारों का सम्मान हो।
P: सार्वजनिक-निजी भागीदारी: नवाचार को बढ़ावा देने और DPI समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
I: समावेशी एवं समतामूलक विकास: सुनिश्चित करें कि DPI की पहल समावेशी और समतामूलक हो तथा हाशिए पर पड़े और कमजोर लोगों सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।
| Read more- Live Mint UPSC Syllabus- GS 2- Government Policies and Interventions for development in Various sectors |